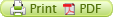आइए, आरक्षण पर चर्चा तक न करें और मनमोहन वैद्य को सूली पर टांग दें!
आरएसएस प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के आरक्षण पर दिये बयान में सामाजिक दृष्टि से तो कुछ भी ग़लत नहीं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसकी टाइमिंग पर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले आरएसएस के बड़े ‘मोहन’ यानी मोहन भागवत ने भी आरक्षण पर ऐसा ही बयान दिया था। अब यूपी चुनाव से पहले उसके छोटे ‘मोहन’ यानी मनमोहन वैद्य के बयान से राजनीतिक तूफ़ान आना तय है।
अब देश को जाति के आधार पर बांट कर राजनीति करने वाले लोग इसका विरोध करेंगे और बीजेपी के नेता ऊपरी तौर पर इस बयान से ख़ुद को अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर छाती पीटेंगे। एक तरफ़ बीजेपी पर आरएसएस से संचालित होने का आरोप लगता है, दूसरी तरफ़ एन चुनावों से पहले आरएसएस की तरफ़ से ऐसे बयान आ जाते हैं, जिनसे भाजपाई भी भौंचक्के रह जाते हैं।
दोनों संगठनों के इस अजीबोगरीब रिश्ते से यूपी चुनाव में यह तो हो सकता है कि अगड़ों के जो वोट दूसरी पार्टियों को पड़ने वाले हैं, वे बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकृत हो जाएं, लेकिन पिछड़ों और दलितों के जिन वोटों की उसे सख्त ज़रूरत है, वे उससे छिटक भी सकते हैं। क्या आरएसएस के नेता भूल गए कि बिहार चुनाव में उनके बयान का क्या असर हुआ था?
या फिर एक थ्योरी जो हवा में है, कहीं वह सच तो नहीं कि आरएसएस बीजेपी को यूपी चुनाव हराना चाहता है? क्या आरएसएस भाजपा के मौजूदा नेतृत्व के कामकाज के तरीके से ख़ुश नहीं है? या फिर वह मानता है कि मोदी सरकार की नीतियां सही रास्ते पर नहीं जा रही हैं? क्या सचमुच आरएसएस के लोग बीजेपी और सरकार में बैठे लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं?
जहां तक मैं समझता हूं कि आरएसएस तात्कालिक वजहों से अपनी नीतियां तय नहीं करता, न ही चुनावों के आने-जाने से उसकी दीर्घकालिक नीतियों पर कोई फ़र्क़ पड़ता है, लेकिन यह भी सही है कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो, तब तक आरएसएस के ज़िम्मेदार नेता किसी भी मुद्दे पर बोलने से बच निकलते हैं। आरएसएस वाचाल नेताओँ से परहेज करता है और विवादास्पद मुद्दों पर उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से मना करता है।
बहरहाल, अब बीजेपी क्या करेगी? क्या वह बिहार चुनाव की तरह डिफेंसिव हो जाएगी या फिर इस मुद्दे पर आरएसएस की जो भावना है, उसे ठीक से समझते हुए आक्रामक तरीके से इस वैचारिक बहस को आगे बढ़ाएगी? चुनाव में जातिगत समीकरणो की मजबूरियो को देखते हुए उसके लिए इसे आगे बढ़ाने का विकल्प तो बहुत मुश्किल है, इसलिए डिफेंसिव ही होना पड़ेगा। लेकिन डिफेंसिव होने से भी क्या होगा? जो नुकसान होना है, वह तो हो ही जाएगा।
दरअसल, आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए ‘आगे कुआं, पीछे खाई’ जैसा बन गया है। अगर वह इस बात को मानती है कि समाज में जातिगत भेदभाव ख़त्म करने और समानता लाने के लिए आरक्षण से इतर दूसरे नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए, तो उन जातियों के वोट से उसे हाथ धोना पड़ेगा, जिनके पास इस वक्त आरक्षण है। और अगर वह इसे अनंतकाल तक यथारूप जारी रखने की नीति अपनाती है, तो आरएसएस के विचारों के यह निश्चित रूप से ख़िलाफ़ होगा।
वैसे, यह भी कम अफ़सोस की बात नहीं है कि कहने को हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिनपर इस देश में बहस नहीं हो सकती। आरक्षण भी एक ऐसा ही मुद्दा है। आख़िर हम क्यों इस बात की समीक्षा नहीं कर सकते कि पिछले 67 साल में इस व्यवस्था से क्या हासिल हुआ और कहां यह फेल हो गई? कोई न कोई चुनाव तो इस देश में हमेशा ही रहता है, तो क्या हम इस गंभीर मुद्दे पर कभी बात न करें?
सच्चाई यह है कि संविधान सभा में भी बहुत सारे नेता आरक्षण के विचार से सहमत नहीं थे और यह मानते थे कि अगर एक बार यह सिलसिला शुरू हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन आशंका के अनुरूप ही, बात अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक नहीं रुकी।
बाद में पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की मांग होने लगी और मंडल की राजनीति ने तूल पकड़ा। आख़िरकार वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर 1991 में पिछड़ों को भी आरक्षण दे दिया। और अब हम देख रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा समेत देश के अलग-अलग राज्यों में कई जातियां आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन पर उतारू हो आई हैं। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद जब-तब धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण की मांग उठती रहती है।
ज़ाहिर तौर पर आरक्षण की खैरात मांगने और बांटने का यह सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। यह तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीलिंग लगा रखी है, वरना तुष्टीकरण और वोट-बैंक पॉलीटिक्स के चक्कर में अब तक तो यह 70-80 प्रतिशत तक पहुंच गया होता। लेकिन इसी राजनीतिक रिस्क के बीच हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि अगर 2016-17 में भी दलितों-पिछड़ों का उत्पीड़न और उनसे भेदभाव मुद्दा बना हुआ है, तो आरक्षण ने पिछले 67 साल में हासिल क्या किया है?
वास्तव में आरक्षण की व्यवस्था जिस तरीके से लागू है, उस तरीके से न तो पिछले 67 साल में यह अपना मकसद हासिल कर पायी है, न अगले 6700 साल में कर पाएगी। जो लोग जातीय आरक्षण से इतर सोचने में राजनीतिक असुरक्षा महसूस करने लगते हैं, उन्हें भी कम से कम इतना तो विचार करना ही चाहिए कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसे दोबारा और फिर बार-बार यह सुविधा क्यों मिलनी चाहिए? अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है, तो ‘एक परिवार, एक बार’ की नीति अपनाने में क्या बुराई है?
सवाल यह भी उठता है कि क्या जाति के नाम पर रामविलास पासवान, मायावती, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव जैसों के परिवार वालों को भी आरक्षण देते रहना उचित है? अगर जातिगत आरक्षण बरकरार भी रखना है, तो क्रीमी लेयर को इससे बाहर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? सवाल है कि क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ़ उन्हें ही नहीं मिलना चाहिए, जो सचमुच कमज़ोर हैं? क्या सक्षम लोगों को सिर्फ़ जाति के नाम पर आरक्षण देते रहना इस व्यवस्था की मूल भावना का मखौल नहीं है? सवाल है कि क्या सबको एक समान शिक्षा और रोज़गार के समान अवसर देकर आरक्षण की ज़रूरत को ख़त्म नहीं किया जा सकता है?
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन मुद्दों पर विचार करने की बात करना भी इस देश में दलित-पिछड़ा विरोधी साबित होना है। आरक्षण के मुद्दे पर हालिया हिंसक आंदोलनों को देखते हुए अगर कोई कहता है कि इससे समाज में अलगवावाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम तो उसे सूली पर ही टांग देंगे। इसलिए आइए, आरक्षण के मुद्दे पर हम चर्चा तक नहीं करते हैं और मनमोहन वैद्य को सूली पर टांग देते हैं।