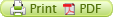माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्या जजों को धार्मिक पहचान देना ज़रूरी है?
तीन तलाक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है और उन्होंने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। यद्यपि हमें उम्मीद है कि वहां से आने वाला फ़ैसला क्रांतिकारी और समाज को नई राह दिखाने वाला होगा, फिर भी एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत को उस तरह से काम नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे राजनीतिक दल करते हैं।
ऐसा लगा कि तीन तलाक के मुद्दे पर विचार करने के लिए बैठते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट भारी दबाव में थे और यह दबाव बाहरी नहीं, बल्कि उनका अपना ओढ़ा हुआ था। शायद उन्हें डर था कि चूंकि सुनवाई का मुद्दा धर्म-विशेष से जुड़ा है, इसलिए कल को लोग उनके फ़ैसले पर सवाल न उठा दें, इसलिए उन्हें भी अपनी पीठ में विभिन्न धर्मों का संतुलन बनाने की ज़रूरत पड़ गई। हम आम नागरिक हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी हो सकते हैं। हमारे राजनीतिक दल भी हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अदालतों और न्यायाधीशों को हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि से ऊपर होना चाहिए।
अब तक हम न्यायाधीशों को उनके जाति या धर्म से जानने-पहचानने के आदी नहीं रहे हैं। हिन्दुओं के फैसले मुस्लिम और मुस्लिमों के फैसले हिन्दू जज सुनाते रहे, लेकिन हमने कभी उनके फैसलों या उनकी नीयत पर संदेह नहीं किया। हमने कभी नहीं सोचा कि वे हिन्दू हैं या मुस्लिम या किसी अन्य जाति-संप्रदाय के, लेकिन इस बार स्वयं सुप्रीम कोर्ट के कदम से अहसास हुआ कि जजों की भी जातियां होती हैं, उनके भी धर्म होते हैं।
तीन तलाक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान पीठ बनाई, उसके बारे में हमने जाना कि इस बेंच में एक जज हिन्दू, एक जज मुस्लिम, एक जज सिख, एक जज ईसाई और एक जज पारसी हैं। हमारे माननीय जजों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पवित्रता से अधिक महत्वपूर्ण उनकी धार्मिक पहचान हो गई। ऐसा लगा, जैसे इस धर्मनिरपेक्ष देश में इतने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने बैठी संविधान पीठ में कोई जज धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, बल्कि अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधि थे। ऐसा लगा, जैसे राजनीतिक दलों पर चुनावों में टिकटों का बंटवारा करते समय विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच संतुलन बनाने का दबाव रहता है, वैसा ही दबाव हमारी सर्वोच्च अदालत भी महसूस कर रही थी।
क्या हमारे देश में विभिन्न धर्मों के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि अब हमें अदालतों में भी इस तरह के संतुलन बनाने पड़ेंगे? अगर हां, तो फिर यह संतुलन आप कहां-कहां बनाएंगे? फिर तो जिन मामलों में मुस्लिम आरोपी हों, उनकी सुनवाई मुस्लिम जजों से करानी होगी। जिन मामलों में हिन्दू आरोपी हों, तो उनकी सुनवाई हिन्दू जजों से करानी होगी। फिर तो कल को कोई मुजरिम भी मुंह उठाकर आरोप लगा सकता है कि चूंकि जज दूसरे धर्म के थे, इसलिए उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई। अगर जज स्वयं अपना धर्म जताने की पहल करेंगे, तो नागरिक तो उनका धर्म देख ही सकते हैं। और जब बात धर्म से शुरू होगी, तो जातियों पर भी जाएगी ही। दलितों के केस सुनने के लिए दलित और पिछड़ों के केस सुनने के लिए पिछड़े जज लगाने पड़ेंगे। शिया के केस सुनने के लिए शिया और सुन्नी के केस सुनने के लिए सुन्नी जज लगाने पड़ेंगे।
हमारा मानना है कि जज की कुर्सी पर बैठने के बाद वे न हिन्दू होते हैं, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। वे सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के संविधान के रक्षक होते हैं। वे एक धर्मनिरपेक्ष देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाले प्रहरी होते हैं। ज़िम्मेदारी का ऐसा बोध जजों में भी रहे और ऐसा अटूट भरोसा नागरिकों में भी रहे, तभी हमारा लोकतंत्र अधिक मज़बूत होगा। लेकिन तीन तलाक की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ के धर्म-आधारित गठन से इस भरोसे को खरोंच पहुंचने का ख़तरा है। कई लोग इसे न्यायिक तुष्टीकरण की संज्ञा भी दे रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण एक तो और अधिक तुष्टीकरण की भूख पैदा करता है, दूसरे आज तक कोई भी इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए सवाल खड़े करने से जिनका हित सधता हो, वे तो इस बेंच पर भी सवाल खड़े कर ही सकते हैं। मसलन,
- तीन तलाक मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा है, इसका वास्ता इस्लाम से है, फ़ैसला संविधान के तहत होना है, तो फिर अन्य धर्मों के उन जजों की इस बेंच में क्या ज़रूरत थी, जिन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं? क्या उन्हें सिर्फ़ दिखावा करने के लिए रखा गया?
- कहने को आपने पांच धर्म के पांच जज बिठा दिए, लेकिन मुस्लिम तो इनमें सिर्फ़ एक थे। यानी अगर फ़ैसला तीन तलाक के ख़िलाफ़ जाता है, तो लोग तो कह ही सकते हैं कि फ़ैसला पहले से तय था और मुस्लिम जज महज दिखावे के लिए रखे गए थे।
- अगर एकमात्र मुस्लिम जज तीन तलाक के पक्ष में हों, तो भी उनका फ़ैसला तब तक नहीं चल सकता, जब तक कि अन्य धर्मों के चार जजों में से कम से कम दो उनसे सहमत न हों। यानी अंतिम फ़ैसला तो दूसरे धर्मों के जजों पर ही निर्भर है, फिर मुस्लिमों से न्याय कितना हुआ?
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंच के एकमात्र मुस्लिम जज अब्दुल नज़ीर ने छह दिन की सुनवाई में विभिन्न पक्षों से एक बार भी जवाब-तलब नहीं किया। यह क्या दर्शाता है? क्या बेंच में उनकी मौजूदगी मात्र को पर्याप्त मान लिया जाना चाहिए?
- फैसला महिलाओं के जीवन का होना है, लेकिन पांच जजों में से एक भी महिला न होने पर पहले ही कई लोग सवाल उठा चुके हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर यह होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या तो
- धार्मिक संतुलन बनाने के पचड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि जज किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं, संविधान का रखवाला होता है।
या फिर
- पांच धर्मों के पांच जजों की बजाय पांच मुस्लिम जजों की पीठ बनाते, जिनमें दो या तीन महिलाएं होतीं। फिर उस पीठ का फ़ैसला अगर तीन तलाक के ख़िलाफ़ भी जाता, तो मुस्लिम समाज में उसकी स्वीकार्यता अधिक होती।
लेकिन चूंकि दूसरा विकल्प अपनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश ही नहीं हैं, इसलिए पहला विकल्प अपनाने में कोई बुराई नहीं थी। जितना ज़रूरी यह है कि हम इस देश के नागरिक माननीय सुप्रीम कोर्ट पर अपना भरोसा बनाए रखें, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि वे स्वयं भी अपने ऊपर और देश के नागरिकों के ऊपर भरोसा बनाए रखें।